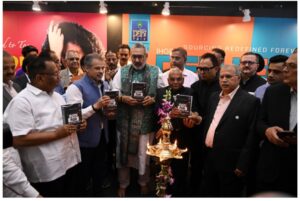मीडिया की तस्वीर ही बदल गई

अनिल निगम
(संपादक, आईआईएमटी न्यूज)
editor@iimtnews.com editor@iimtnews.com
https://twitter.com/AnilNigam12
https://www.facebook.com/anil.nigam.98
भारत की आजादी में मीडिया की अहम भूमिका रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिस तरह से मीडिया का उद्भव और विकास हुआ, उसी के चलते पत्रकारिता मिशनरी बन गई। मीडिया खासतौर से भाषायी पत्रकारिता ने संपूर्ण भारत वर्ष में अंग्रेजी शासन की कुनीतियों, उत्पीड़न, शोषण और अराजकता को उजागर कर जनजागरण और राष्ट्रवाद की भावना का संचार किया, उसी के चलते प्रेस ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वमेय चौथे स्तम्भ का दर्जा हासिल कर लिया। लेकिन आजादी के बाद मीडिया के स्वरूप और भूमिका में बहुत तेजी से बदलाव हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऑनलाइन मीडिया के बढ़ते प्रभाव के चलते पत्रकारिता की दशा और दिशा पूरी तरह से बदलने लगी है। जहां पहले अखबार और पत्रिकाएं सर्वाधिक शक्तिशाली होती थीं, वहीं अब मोबाइल, टैब और टीवी ताकत बहुत तेजी से बढ़ गई है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में इसकी पुष्टि भी हो गई है।
आजादी के बाद प्रेस को भी आजादी मिली। संविधान में अनुच्छेद 19 (A) के तहत हर नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार मिला। समाचार-पत्रों के पंजीयन में छूट मिलने के कारण सैकड़ों पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। वर्ष 1950 के बाद पत्रकारों ने बिगड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में अहम भूमिका अदा की। पत्रकारों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए 1952 में प्रेस कमीशन और 1966 में प्रेस परिषद बनाई गई।
वर्ष 1962 में भारत-चीन और 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान पत्रकारिता का देश और समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण सकारात्मक योगदान रहा। वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में लगे आपातकाल में प्रेस की आजादी पर कुठाराघात हुआ। प्रेस पर सेंसर लागू कर दिया गया। लेकिन टीवी और सैटेलाइट के आ जाने से पत्रकारिता का स्वरूप ही बदल गया। 1980 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव बढ़ा। इसका नकारात्मक पहलू यह रहा कि वर्ष 2000 आते-आते एक तरफा खबरें और पीत पत्रकारिता के मामले भी तेजी से बढ़ गए।
ध्यातव्य है कि तकनीकी विकास के साथ ही वर्ष 2000 में भारत में भी ऑनलाइन मीडिया एवं सोशल मीडिया का प्रदुर्भाव हुआ। आज भारत में 70 करोड़ लोगों के पास फोन हैं। 25 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। 25 करोड़ लोगो में से 15 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। आज सोशल मीडिया हर नागरिक की अभिव्यक्ति का सशक्त साधन बन गया है। वह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगा है। इसका सबसे बड़ा लाभ है कि हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, प्रियजनों से सीधा संपर्क में रह सकते हैं। इसके अलावा हमें खबरें और सूचनाएं भी बहुत तेजी से प्राप्त होती हैं।
आजकल क्रिकेट, शायरी, फिल्म जगत, बागवानी, खाना पकाना (पाक कला), बागवानी के शौक़ीन लोग अपने ग्रुप बनाकर अपने शौक को पूरा कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया ज्ञान का नया भंडार बन गया है। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बिजनेस, व्यापार का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में लोगों, राजनैतिक दलों एवं अन्य समूहों ने जिस तरीके से फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्एप पर अभियान छेड़े, उससे यह साबित होता है कि वर्तमान में सोशल मीडिया की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी है।
हालांकि सोशल मीडिया का मनमाने तरीके से इस्तेमाल भी हो रहा है। उसके नुकसान भी काफी हैं। समाज में लाखों लोगों को इसकी लत लग चुकी है। वे अपने जरूरी काम छोड़कर इसमें घंटों लगे रहते हैं। कई बार फेक न्यूज के माध्यम से सोशल मीडिया अफवाहें फैलाई जाती हैं। इससे समाज में अशांति तक फैल जाती है। इसके अत्यधिक इस्तेमाल के चलते बच्चे अपनी पढाई से जी चुराने लगे हैं। देर तक के इस्तेमाल से उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं। एक अनुमान के अनुसार बच्चे से लेकर बड़े तक रोज 3 से 4 घंटे सोशल मीडिया पर देते हैं।
मीडिया की वर्तमान भूमिका पर कोई निष्कर्ष निकालने से पहले हमें एक बार फिर यह समझने की जरूरत है कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व वर्ष 1857 की क्रांति ने भारत में राष्ट्रीय जागरण के युग का प्रारंभ कर दिया था। उन्नसवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ही विभिन्न भाषाओं में समाचार पत्र-पत्रिकाओं ने नवचेतना का संचार करना शुरू कर दिया। राष्ट्रवादी विचारों के पत्रकारों, संपादकों और लेखकों ने संपादकीय, लेखों और खबरों के माध्यम से ब्रिटिश शासन के कुशासन को उजागर किया। देश में पहले प्रिंटेड समाचार-पत्र बंगाल गजट की शुरुआत आयलैंड के जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने वर्ष 1780 में कोलकाता से की थी। लेकिन दो वर्ष बाद ही इस समाचार-पत्र को बंद करा दिया गया।
कानपुर के साहित्यकार पंडित जुगल किशोर सुकुल ने 30 मई 1826 को हिंदी भाषा का पहला समाचार-पत्र-उदन्त मार्तण्ड प्रकाशित करना शुरू किया। उदन्त मार्तण्ड में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ व्यंग और खड़ी बोली की भाषा में लिखा जा रहा था, इसलिए अंग्रेजों को पहले तो अखबार के मंसूबों का आभास नहीं हो सका, लेकिन कुछ समय बाद जब उनको पता चला कि जनता में जो क्रांति की भावना पैदा हो रही है, उसके पीछे इस अख़बार की भूमिका है, तो उन्होंने अखबार की डाक ड्यूटी बढ़ा दी। इसका सीधा प्रभाव समाचार-पत्र की आर्थिक स्थिति पर पड़ा और भारत के पहले हिंदी अख़बार का प्रकाशन 4 दिसंबर 1827 को बंद हो गया।
समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय ने भारतीय समाज में अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ अपने अखबारों के माध्यम से गंभीर प्रहार किए और जनता में जागरूकता पैदा की। उन्होंने ब्रह्मिनिकल मैग्ज़ीन (अंग्रेजी), संवाद कौमुदी (बांग्ला) और मिरातुल-उल-अख़बार (फारसी) अखबारों का संपादन और प्रकाशन किया। हालांकि राजा राममोहन राय ने 4 अप्रैल 1823 को मिरात-उल-अख़बार और संवाद कौमुदी का प्रकाशन बंद कर दिया।
सरदार भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन का प्रारंभ प्रताप नामक अख़बार से हुआ था। प्रताप का प्रकाशन सुधारवादी नेता गणेशशंकर विद्यार्थी करते थे। प्रताप में प्रकाशित लेखों के कारण संपादक गणेशशंकर विद्यार्थी को 5 बार जेल जाना पड़ा था। भारत में क्रांतिकारी पत्रकारिता की नींव लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने रखी थी। उन्होंने 1881 में मराठी भाषा में ‘केसरी’ और अंग्रेजी में ‘मराठा’ नामक साप्ताहिक अखबारों से जुड़े और उनका संपादन किया। कोल्हापुर के दीवान के बारे में लिखने के कारण उन पर मानहानि का केस हुआ और उनके सहायक अश्रेकर को जेल जाना पड़ा।
राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत में ‘यंग इंडिया’ और ‘नवजीवन’ समाचार-पत्रों का संपादन और प्रकाशन किया। उनकी पत्रकारिता का प्रमुख उद्देश्य संपूर्ण भारत में सद्भावना फैलाना और देश के युवाओं समुचित दिशा प्रदान करना था, लेकिन ब्रिटिश शासन के प्रेस विरोधी कानूनों और नीतियों के चलते इनका प्रकाशन बंद करना पड़ा। गांधीजी ने 1933 में समाज के उपेक्षित एवं अस्पृश्य वर्ग को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए अंग्रेजी भाषा में ‘हरिजन’, हिंदी में ‘हरिजन सेवक’ तथा गुजराती में ‘हरिबंधु’ नामक समाचार-पत्रों का प्रकाशन किया मगर ये अख़बार स्वतंत्रता के पश्चात बंद हो गए।
नि:संदेह, भारत की आजादी में मीडिया ने अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी। मगर हमारे देश में 60 वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस सरकार की यह विडंबना रही है कि उसने पत्रकारिता के लिए समर्पित स्वतंत्रता सेनानियों और समाचार-पत्रों के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। यही कारण है कि समाजसेवा और देशभक्ति जैसे बीजो को अंकुरित करने वाले इन स्वतंत्रता सेनानी अखबारों का आज कोई वजूद नहीं है। आज इन अखबारों की जगह टीवी और मोबाइल लेता जा रहा है। ऑनलाइन मीडिया अभी लोगों के बीच अपना संपूर्ण भरोसा तो कायम नहीं कर पाया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में ऑनलाइन एवं सोशल मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिस तरीके से सक्रिय भूमिका निभाई है, उससे इस मीडिया का प्रभाव तो बढ़ा है।